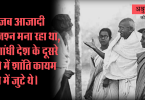प्रताप नारायण सिंह II
किसान जीवन के यथार्थ को गुप्तजी ने बिना किसी अतीत का सहारा लिए ठोस सामाजिक भूमिका पर रखकर निर्मित किया है। कहा जा सकता है कि ‘किसान’ (1915) खण्ड काव्य के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और किसान के जीवन को वे एक मुख्य प्रश्न बनाकर चिंताओं के केन्द्र में लाये। इसका कारण रहा होगा 19वीं सदी में देश में किसानों की बदतर जीवन स्थिति। जमींदारी प्रथा के चलते किसानों के जीवन की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि वे खेत मजदूर बनकर भी रोजी-रोटी पूरी नहीं कर पाते थे। इसलिए रोजी-रोटी की तलाश में उन्हें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा और अनेक किसान शर्तबंद कुली बनाकर भारत से बाहर फीजी, मारिशस, ट्रिनीडाड आदि द्वीपों पर भेजे जाने लगे।
इस पर देश में राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूरों पर होने वाले अत्याचारों का गांधी जी ने विरोध किया। 1914 में तातेराम सनाद्य के फीजी संस्मरणों को श्री बनारसीदास चतुर्वेदी ने फीजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष शीर्षक से लिखा। यह पुस्तक बहुत चर्चित हुई और अंग्रेजी सरकार से यह माँग की जाने लगी कि वह भारतीय किसान मजदूरों को विदेश भेजना बंद करे और भेजे गये मजदूरों को वापस बुलाया जाए। इसी अवसर पर गुप्त जी ने “किसान” खण्डकाव्य लिखा। इसकी प्रेरणा गुप्त जी को द्विवेदी जी के किसानों की हालत का बयान करने वाले निबंधों से मिली होगी, हालाँकि देश की वस्तुस्थिति किसी से भी छिपी नहीं थी। भारतीय जीवन की आधारभूत आर्थिक नींव खेती ही रही है। अंग्रेजी सत्ता के शोषण के चक्र – बल से सबसे अधिक नुकसान सामान्य किसानों का ही हुआ।
अंग्रेज, मनसबदार, बड़े बड़े जमींदार, नवाब, रैयतदार इन सब के शोषण का शिकार वह किसान ही बना जो अपनी मेहनत से जमीन जोत कर दो जून की रोटी की व्यवस्था करता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने “संपत्तिशास्त्र’ नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में किसानी जीवन का उल्लेख करते हुए उन्होंने लिखा: “खेतिहरों का व्यवसाय या पेशा खेती करना है और खेती खेतों में होती है। हिन्दी प्रांतों में जितनी भूमि खेती करने लायक है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी के मालिक जमींदार, ताल्लुकेदार, नंबरदार और राजा रईश बन बैठे हैं। वे काश्तकारों से खूब लगान लेते हैं, उसे समय-समय पर बढ़ाते भी हैं और कारण उपस्थित हो जाने पर उन्हें खेतों से बेदखल भी कर देते हैं। इस संबंध में जो कानून बने हैं वे काश्तकारों के सुभीते के कम और जमींदारों के सुभीते के अधिक हैं| जब पैदावार बहुत कम हो जाती है और लगान बेबाक नहीं होता तब ऋण लेना पड़ता है। ऋण की मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है और एक दिन घर द्वार, बैल बछिया सब नीलाम हो जाते हैं। खेती ही प्रधान व्यवसाय ठहरा।’
इसी प्रकार उन्हीं दिनों “सरस्वती’ में किसान जीवन पर अन्य लेखकों के भी सारगर्भित लेख, निबंध छपते रहते थे। गुप्त जी की दृष्टि से भी किसानी जीवन अछूता नहीं था। वे भी यह जानते थे कि किसानों की ऐसी हालत का कारण अंग्रेजी सरकार की यहाँ से अन्न विदेशों में ले जाने की नीति ही थी। “भारत-भारती’ में इसका वर्णन वे यूँ करते हैं :
“अब पूर्व की-सी अन्न की होती नहीं उत्पत्ति है
पर क्या इसी से अब हमारी घट रही संपत्ति है?
यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो,
तो देश फिर सम्पन्न हो, क्रंदन रुके, आनंद हो।
अंग्रेजों के साथ-साथ गुप्त जी महाजनों को भी किसानों की ऐसी बदहाली के लिए जिम्मेवार ठहराते हैं :
हेमंत में बहधा घनों से पूर्ण रहता व्योम है,
पावस निशाओं में तथा हँसता शरद का सोम है
हो जाय अच्छी भी फसल पर लाभ कृषकों को कहाँ?
खाते सवाई, बीज ऋण से हैं रंगे रक्खे कहाँ?
आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में
अधपेट खाकर फिर उन्हें है काँपना हेमन्त में।
लेकिन भारतीय किसान विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता और पूरी कर्मठता से श्रम में लीन रहता है। इसका चित्रण करना भी गुप्त जी नहीं भूलते :
बरसा रहा है रवि अनल भूतल तवा- सा जल रहा,
है चल रहा सन- सन पवन, तन से पसीना बह रहा,
देखो कृषक शोणित सुखाकर हल तथापि चला रहे,
किस लोभ से इस अर्चि में वे निज शरीर जला रहे।
मध्याह्न उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुँची वहीं, ,
हैं रोटियाँ रूखी, खबर है शाक की उनको नहीं।
संतोष से खाकर उन्हें वे, काम में फिर लग गये ,
भरपेट भोजन पा गये तो भाग्य मानो जग गये।
“भारत-भारती” के अलावा किसानों के जीवन पर केंद्रित ‘किसान’ खण्डकाव्य गुप्त जी की ऐसी रचना है जो इतिहास, पुराण का सहारा नहीं लेती बल्कि सीधे-सीधे किसानों के सामाजिक यथार्थ को हूबहू हमारे सामने प्रस्तुत करती है। इसमें विस्तार से गुप्त जी ने किसान जीवन की दुर्दशा को संवेदनात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस खण्डकाव्य को कवि ने आठ सर्गों में बाँटा है, जिसमें आत्मचरितात्मक रूप में किसान जीवन की कथा “प्रार्थना’ से शुरु होकर “बाल्य और विवाह”, “गार्हस्थ’, “सर्वस्यान्त”, “देश त्याग”, “फिजी”, “प्रत्यावर्तन” और “अंत” शीर्षकों में पूरी होती है। “प्रार्थना” सर्ग में प्रथम विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में भारतीय किसान की दुर्दशा का चित्रण है :
कृषि ही थी तो विभो बैल ही हम को करते,
करके दिनभर काम शाम को चारा चरते।
कुत्ते भी हैं किसी भाँति दग्धोदर भरते,
करके अन्नोत्पन्न हमीं हैं भूखों मरते।
प्रभुवर हम क्या कहें कि कैसे दिन भरते हैं?
अपराधी की भाँति सदा सबसे डरते हैं।
याद यहाँ पर हमें नहीं यम भी करते हैं
फिजी आदि में अन्त समय जाकर मरते हैं।
(1850 के लगभग फिजी, ट्रिनीडाड और मारिशस आदि द्वीपों पर खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज़ भारतीय मजदूर किसानों को ले जाने लगे थे। कुछ रास्ते में ही मर जाते थे। वहाँ पर भी उन्हें दयनीय जीवन बिताना पड़ता था। वापिस आना संभव नहीं था। इन्हीं मज़दूर किसानों की मेहनत के बल पर ये द्वीप आज फल फूल रहे हैं और इन्हीं की संतानें आज वहाँ रह भी रही हैं।)
इसी प्रकार “बाल्य और विवाह” में किसान के कैशोर्य जीवन का चित्रण है, “सर्वस्वान्त” में किसान के हृदय की चीत्कार सुनाई पड़ती है। फिजी में किसानों द्वारा देश छोड़ अनजाने द्वीपों पर पापी पेट की खातिर जाने की व्यथा का मार्मिक वर्णन है। कुल मिलाकर किसान कृति भारतीय किसान के वास्तविक जीवन की पीड़ा को एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर सामने रखती है।